छंद किसे कहते हैं- मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छन्द कहते हैं।
जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छन्द द्वारा पद्य का। छन्द का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छन्द शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। पिंगलाचार्य के छन्दसूत्र में छन्द का सुसम्बद्ध वर्णन होने के कारण इसे छन्द शास्त्र का आदि ग्रन्थ माना जाता है। इसी आधार पर छन्द शास्त्र को ‘पिंगलशास्त्र’ भी कहते हैं।
छंद किसे कहते हैं?
छन्द की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियाँ छन्द कहलाती हैं।
छन्द के अंग
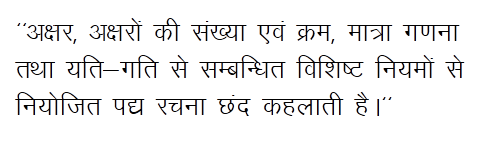
1. वर्ण- वर्ण के दो प्रकार होते हैं-ह्रस्व वर्ण (अ, इ, उ, चन्द्र बिन्दु) और दीर्घ वर्ण (आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग) हस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की दो मात्राएँ।
2. मात्रा – मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह (1) तथा दीर्घ मात्रा का चिन्ह (5), मात्रिक छन्दों में मात्रा गिनकर ही छन्दों की पहचान की जाती है।
3. यति- छन्द को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अन्त में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को ‘यति’ कहते हैं।
4. गति – कविता के कर्णमधुर प्रवाह को ‘गति’ कहते हैं। प्रत्येक छन्द की अपनी एक लय होती है।
5. पाद या चरण- प्रत्येक छन्द में कम से कम चार चरण होते हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति अर्थात् छन्द के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। चरण को पद या पाद भी कहते हैं।
6. तुक – चरण के अन्त में आने वाले समान वर्णों को ‘तुक’ कहते हैं। जैसे तासू- जासु ताके जाके आदि ।
7. गण- तीन-तीन वर्णों के समूह को ‘गण’ कहा जाता है। ‘यमाताराजभानसलगा’ सूत्र के आधार पर गणों की संख्या आ. है, वर्णिक छन्दों की पहचान इसी के आधार पर होती है।
| गण | चिह्न | उदाहरण | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| यगण (य) | ।ऽऽ | नहाना | शुभ |
| मगण (मा) | ऽऽऽ | आजादी | शुभ |
| तगण (ता) | ऽऽ। | चालाक | अशुभ |
| रगण (रा) | ऽ।ऽ | पालना | अशुभ |
| जगण (ज) | ।ऽ। | करील | अशुभ |
| भगण (भा) | ऽ।। | बादल | शुभ |
| नगण (न) | ।।। | कमल | शुभ |
| सगण (स) | ।।ऽ | कमला | अशुभ |

Alankar In Hindi | अलंकार: परिभाषा, भेद, उदाहरण- 2023 | Best For Hindi Sahitya
छन्द के भेद
छन्दों के मुख्यतया दो भेद होते हैं- (1) मात्रिक (2) वर्णिक

- मात्रिक छन्द- जिन छन्दों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है, वे मात्रिक छन्द होते हैं। इनमें मात्राओं की समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे-दोहा, चौपाई, सोरठा आदि।
- वर्णिक छन्द- जिन छन्दों की पहचान के लिये वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है। इसमें वर्णों की संख्या, क्रम और स्थानादि नियम नियन्त्रित रहते हैं। इन्हें वर्णिक छन्द कहते हैं। जैसे-इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि।
मात्रिक और वर्णिक छन्द के पुनः तीन भेद और किये जा सकते हैं।
(1) सम (2) अर्धसम (3) विषम
(1) सम- जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो।
(2) अर्धसम- जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों में एवं द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो।
(3) विषम- जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या अथवा मात्राओं में असमानता
आधुनिक हिन्दी कविता के आधार पर एक तीसरे प्रकार के छन्द को मान्यता मिली। जिसे ‘मुक्त’ छन्द कहा गया। इस छन्द के चरणों में वर्णों एवं मात्राओं में किसी
का भी ध्यान नहीं रखा जाता तथा केवल लय का विधान होता है। जैसे-निराला और अज्ञेय आदि आधुनिक कवियों की कविताएँ।
छन्दों का विवरण
छन्दों की संख्या अनन्त है। अधिक प्रचलित एवं साधारण छन्दों का वर्णन निम्न प्रकार से हैं।
मात्रिक छन्दों के भेद

दोहा
इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएँ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, यह अर्द्ध-सम मात्रिक छन्द है, जैसे-
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ ।
जा तन की झाई परे, स्यामु हरित दुति होइ ।
सोरठा
यह अर्द्ध-सम मात्रिक छन्द है, इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11- मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, यह दोहे का उल्टा होता है, जैसे-
सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे
बिहसे करुणाएन, चितह जानकी लखन तन ॥
चौपाई
यह एक सम मात्रिक छन्द है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में दो गुरु शुभ माने जाते हैं; जैसे-
बंदउ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ।।
अमिय मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू ॥
रोला
इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएँ होती हैं; जैसे-
मूलन ही की जहाँ, अधोगति केसव गाइय ।
होत हुतासन घूम, नगर एकै गलिनाइय ॥
दुर्गति दुर्जन ही जो कुटिल गति सरितन ही में।
फल को अभिलाष, प्रकट कुल कवि के जी में
कुण्डलिया
दोहा और रोला छन्द को मिलाने से कुण्डलिया छन्द बनता है, प्रथम दो पंक्तियाँ दोहा छन्द की तथा अन्तिम चार पंक्तियाँ रोला छन्द की होती हैं, इसमें चौथा चरण पाँचवें चरण में यथावत् आता है। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति 24- 24 मात्राएँ होती हैं जैसे-
कृतघन कबहुँ न मानही, कोटि करी जो कोय।
सरबस आगे राखिए, तक न अपनी होय।
तऊ न अपनी होय, भले की भली न माने।
काम काहि चुप रहे, फेरि तिहि नहिं पहिचाने।
कह गिरधर कविराय, रहत नित ही निर्भय मन ।
मित्र शत्रु न एक, दाम के लालच कृतघन ।
हरिगीतिका
हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 16/12 के विराम से 28 मात्राएँ होती हैं। यह एक सम मात्रिक छन्द है; यथा-
अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी, दण्ड देना धर्म है।
इस बात पर ही पाण्डवों का, कौरवों से रण हुआ,
जो भव्य भारतवर्ष के, कल्पान्त का कारण हुआ।
छप्पय
यह छन्द रोला एवं उल्लाला नामक दो छन्दों को मिलकर बनता है। इसमें छ: चरण होते हैं। पहले चार चरण रोला छन्द के तथा अन्तिम दो चरण उल्लाला छन्द के होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छन्द है; जैसे-
नीलाम्बर परिधान, हरित पट पर सुन्दर है,
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है।
नदियाँ होम प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं,
बन्दीजन खगवृन्द, शेषफन सिंहासन है।
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की,
हे मातृभूमि! तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की।
उल्लाला
यह मात्रिक अर्धसम छन्द है। इसके विषम चरण में 15 और सम में मात्राएँ होती हैं। इस प्रकार यह 28 मात्राओं का छन्द है।
हे शरणदायिनी देवि! तू करती सबका त्राण है।
तू मातृभूमि, सन्तान हमें, तू जननी, तू प्राण है।
गीतिका छन्द
यह मात्रिक सम छन्द है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएँ होती हैं। 14, 12 पर यति । अन्त में लघु गुरु का विधान है।
जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में
कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही,
किन्तु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है,
पूछ उनसे, क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है?
बरवै
यह एक अर्द्धसम मात्रिक छन्द है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएँ होती हैं; जैसे-
अवधि शिला का उस पर था गुरु भार
तिल तिल काट रही थी, दुग जल धार॥
संदर्भ-
छंद किसे कहते हैं- https://hi.wikipedia.org/

